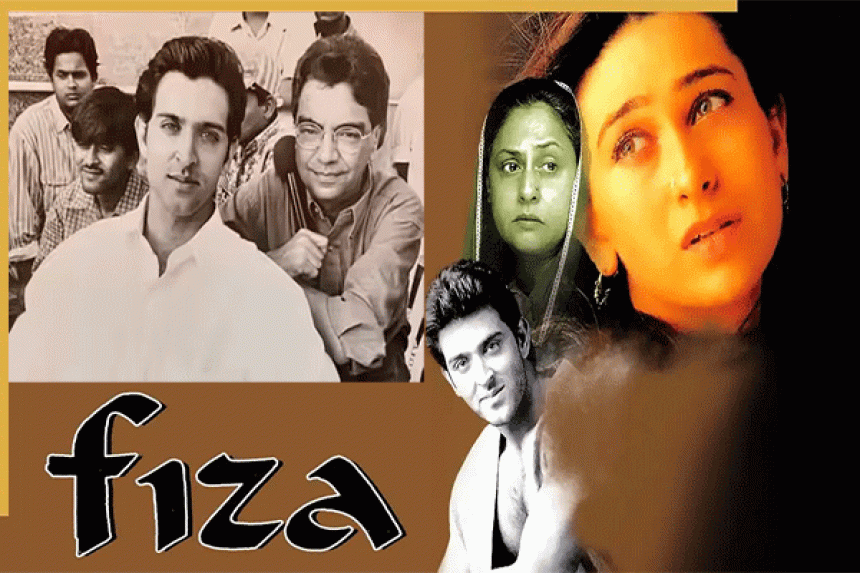
मुंबई: फ़िज़ा की रिलीज़ के 25 साल पूरे होने पर, निर्देशक खालिद मोहम्मद (director Khalid Mohamed) फ़िल्म के निर्माण, उसके विषयों और उसके स्थायी प्रभाव पर विचार करते हैं। सितारों से सजी कलाकारों से लेकर संवेदनशील सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों (sensitive socio-political issues) को उठाने तक, मोहम्मद अपने अनुभवों, प्रेरणाओं और इस कहानी को पर्दे पर लाने के दौरान आई चुनौतियों को साझा करते हैं। इस बेबाक बातचीत में, वह "फ़िज़ा (Fiza)" के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं, एक ऐसी फ़िल्म जो दशकों बाद भी प्रासंगिक बनी हुई है।
एक फ़िल्म निर्माता के रूप में आप उस अनुभव को कैसे देखते हैं?
असंयमी लगने के जोखिम पर, हाँ, मुझे लगता है कि सिनेमाई और विषय-वस्तु के लिहाज से—1992-93 के दंगों के नतीजों के बीच—मुझे लगता है कि फ़िज़ा के निर्देशन में हाथ डाले बिना मैं अधूरा और यहाँ तक कि बेकार होता। ए आर रहमान (A R Rahman) द्वारा रचित कव्वाली पिया हाजी अली का गीत और फिल्मांकन, धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण तत्व की पुष्टि के रूप में सोचा गया था, उम्मीद है कि इसने प्रभाव डाला होगा, जैसा कि अंतर्निहित संदेश ने किया कि समुदायों के ध्रुवीकरण के पीछे विभिन्न निहित राजनीतिक हित हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
एक फिल्म निर्माता के रूप में आपकी प्रेरणा कौन थे?
निर्देशक कोस्टा-गावरस (Z and State of Siege) के काम से प्रेरित होकर, मैंने उनकी गति और संपादन शैली को बनाए रखा, जिसमें श्रीकर प्रसाद के संपादन, संतोष सिवन की छायांकन और रंजीत बारोट के पृष्ठभूमि संगीत ने काफी मदद की, जिनका योगदान फिल्म की शुरुआत में माँ (मेरे दिवंगत दादा) को समर्पित होने के साथ बेहद संवेदनशील है। कुल मिलाकर अनुभव बहुत अच्छा रहा, बेशक कई मुश्किलें आईं, लेकिन मैं शांत रहा। फ़िज़ा तो बननी ही थी।
समीक्षाएँ काफ़ी आक्रामक थीं?
आज तक, मैं समझ नहीं पाया कि पत्रकार बिरादरी इतनी आक्रामक क्यों थी, और मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर, फ़िल्म को नहीं, ऐसी समीक्षाएं क्यों दे रही थी। प्रतिष्ठित व्यापार पत्रिकाओं ने इसे फ्लॉप घोषित कर दिया, जबकि अगर आप बॉक्स-ऑफ़िस कलेक्शन गूगल करें तो यह 7 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और 32 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी। बहरहाल, श्याम बेनेगल सर और फ़िज़ा के लिए लिखी गई मम्मो और ज़ुबैदा की पटकथाएँ ही आज तक मेरी पहचान हैं। इसके अलावा, मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेरिस की अपनी यात्रा के दौरान, जहाँ वे ठहरे थे, मैंने कोस्टा-गावरास से बात की थी और पूछा था कि क्या आतंकवाद-विरोधी आवाज़ उठाने वाली फ़िल्म बनाने का कोई तुक है और उन्होंने जवाब दिया था, "कभी भी काफ़ी नहीं हो सकता। इस विषय पर बनी हर फ़िल्म मायने रखती है, कृपया आत्म-संदेह न करें।"
फ़िल्म में आपके पसंदीदा कलाकार थे: जया बच्चन, ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन... , क्या यह मनमोहन देसाई की मल्टीस्टारर फ़िल्म है?
मनमोहन देसाई से तुलना एक मज़ाक है। उस समय मेरे कोई भी अभिनेता बड़े सुपरस्टार नहीं थे। श्री बच्चन और शाहरुख़ खान कैमियो करने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि यह बनावटी और बेवजह का व्यावसायिक पहलू होगा, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट से उनका रोल हटा दिया। जया जी, जो एक सख़्त ज़िम्मेदार थीं, ने स्क्रिप्ट पढ़ी और अपनी मंज़ूरी दे दी। मुझे याद है कि ऋतिक रोशन, जो कहो ना...प्यार है! पूरी कर रहे थे, ने स्क्रिप्ट पढ़ी और एक घंटे बाद उन्होंने "हाँ" कहा। मैं "भगवान दादा" में एक बाल कलाकार के रूप में उनके अभिनय से दंग रह गया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आँखें इतनी भावपूर्ण हैं कि वे अमन के रूप में अपनी पीड़ा को लिखित संवादों से कहीं आगे तक व्यक्त कर सकते थे।
अमन के रूप में उनके अभिनय का ज़िक्र आज कम ही होता है, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा अनमोल रहेगा। करिश्मा कपूर को "ज़ुबैदा" और "फ़िज़ा" की स्क्रिप्ट एक साथ ऑफर की गई थी। उस समय उन्हें "मोहब्बतें" में ऐश्वर्या राय वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर से मेरी किस्मत अच्छी रही। उन्होंने दोनों ही काम किए, और उन्हें सबसे मुश्किल सीन—खासकर उनकी दबी हुई चीख और एक अख़बार के संपादक के साथ वाला सीन, जिसे वे डाँटती हैं—करते हुए देखना न सिर्फ़ मेरे लिए, बल्कि पूरी टीम के लिए भी दंग रह गया। जहाँ तक मनोज बाजपेयी और सुष्मिता सेन की बात है, दोनों ने तुरंत हामी भर दी थी।
सुष्मिता ने "मस्त महाउल" की स्क्रैच रिकॉर्डिंग सुनी थी...और तीन दिनों में उदयपुर में कम से कम छह-सात अलग-अलग लोकेशन्स पर इस गाने की शूटिंग की, बीच-बीच में अपनी कार में झपकी भी ली। खैर, यह कोई औपचारिक स्टार प्रोजेक्ट नहीं था...जब हमने शुरुआत की थी तब करिश्मा सबसे बड़ी स्टार थीं। और "फ़िज़ा" की शूटिंग के बीच ही "कहो ना प्यार है" से ऋतिक रातोंरात मशहूर हो गए। उन पर स्टारडम का कोई असर नहीं पड़ा, और वे बंबई के दूर-दराज़ लोकेशन्स पर शूटिंग के लिए मानसून की बाढ़ में भी पैदल जाते थे।
क्या ये सभी आपकी पहली पसंद थे? क्या किसी ने आपको सच में मना किया था?
नादिरा ज़हीर बब्बर ने विनम्रता से वह किरदार निभाने से इनकार कर दिया, जिसे अंततः आशा सचदेव ने बखूबी निभाया। और एक अजीब वाकया हुआ: मेरे सह-निर्माता प्रदीप गुहा ने कहा कि अक्षय कुमार इसमें रुचि रखते हैं, हालाँकि मैं नहीं थी। मैंने उन्हें वह किरदार निभाने के लिए स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाई, जिसे बाद में बिक्रम सलूजा ने निभाया। अक्षय, फिज़ा के भाई, अमान का किरदार निभाना चाहते थे। मैं जितनी जल्दी हो सके उनके ऑफिस से भाग निकला। यह एक घोर गलत कास्टिंग होती।
इतने बड़े कलाकारों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था?
कलाकार सहयोगी थे। निर्देशन में यह मेरा पहला प्रयास था, और मुझे याद है कि जयाजी ने एक बार मुझसे पूछा था, "तुम इतने शांत कैसे रह रहे हो?" यह व्यावहारिक नहीं लगता, लेकिन मैं शांत थी क्योंकि मैं जानती थी कि ऊपर कोई मुझे पसंद करता है, मेरी दादी, जिनकी यादें मेरे अंदर घूमती रहती थीं। मेरे लिए उनके आखिरी शब्द थे, "कभी किसी मोहताज मत बनना।" बेशक, मैं पूरी तरह से उच्च-स्तरीय टीम पर निर्भर था। और हाँ, मुझे कुछ दृश्यों के लिए 100 से ज़्यादा लोगों की टीम का नेतृत्व करना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं कोई रिंगमास्टर नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो फिल्म निर्देशन साँस लेने जितना ही स्वाभाविक हो सकता है। मैं बस एक बार उदयपुर में "मस्त महाउल" की शूटिंग के दौरान थोड़ा हैरान हुआ था, जिसमें ऋतिक के कुछ अंश शामिल थे। वह पूरे देश में छा गए थे और कलेक्टर से लेकर बड़े पुलिस अधिकारी तक, हर कोई उनके लिए पार्टियाँ आयोजित करना चाहता था। यह संभव नहीं था। इसलिए गाने की शूटिंग गुरिल्ला स्टाइल में की गई थी, हम हर तरह की जगहों पर गए, जैसे किसी बड़े कुएँ वाले खेत में और ईंट के भट्टों में। और जब ऋतिक को कोई एक्शन सीन करना होता था, तो मैं अपनी आँखें बंद कर लेता था। वह इसे इतनी वास्तविकता से करने में माहिर था कि उसे चोट लग जाती थी, जैसे एक बार चाकू लगने से उसके हाथ से खून बहने लगा था, लेकिन वह बेफिक्र रहा, थोड़ा एंटीसेप्टिक लगाया और बिना मुँह बनाए काम जारी रखा।
फ़िज़ा ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो आज पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है: मुस्लिम पहचान। आज आप फ़िज़ा के बारे में कितना गहराई से महसूस करते हैं?
मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। बढ़ते अलगाव और गैर-समावेशीपन से मैं टूटा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने सिर्फ़ मुस्लिम किरदारों और उनकी परिस्थितियों, उनके इर्द-गिर्द की 'फ़िज़ा' पर आधारित फ़िल्में निर्देशित और लिखी हैं। आज कोई भी फ़ाइनेंसर/निर्माता उन्हें नहीं चाहता। तो कम से कम पर्दे पर तो मेरी कहानियाँ यहीं ख़त्म।
आज भी यह आम धारणा है कि पत्रकार ही अयोग्य फ़िल्म निर्माता बनते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने उन्हें ग़लत साबित कर दिया?
आप पत्रकारिता के पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं था या किसी को सही या ग़लत साबित करने का कोई इरादा नहीं था। अगर ज़्यादातर, ख़ासकर स्टारडस्ट, इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे ने फ़िल्म की आलोचना की, तो कोई बात नहीं। सबसे निराशाजनक समीक्षा विद्वान मैथिली राव की थी, जिन्होंने ब्रिटेन की बेहतरीन पत्रिका, साइट एंड साउंड में लिखा था, इस बात से हैरान कि मणि कौल की फ़िल्में पसंद करने वाला कोई व्यक्ति कैसे पलट सकता है। वह भूल गईं कि मैं मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा, दोनों का प्रशंसक रहा हूँ। शायद मुझे उन्हें संजय लीला भंसाली की "खामोशी: द म्यूजिकल", आदित्य चोपड़ा की "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे" और करण जौहर की "कुछ कुछ होता है" की अपनी समीक्षाएं भेजनी चाहिए थीं। लेकिन रहने दो, हर किसी की अपनी पसंद होती है।
आखिरकार, आप फिल्मी दुनिया से इतने दूर क्यों हैं?
मैं तब से दूर हूँ जब से मुझे श्रद्धांजलि, पुरानी यादें ताज़ा करने वाले लेख और देश की अनजाने या सोची-समझी प्रोपेगैंडा फिल्मों की भरमार लिखने का काम सौंपा गया था। भगवान के लिए, सच तो यह है कि जब आप खुद कुर्सी पर नहीं होते, तो आपको उनकी ज़रूरत उनसे ज़्यादा होती है जितनी उन्हें आपकी। तो नहीं, शुक्रिया। सुभाष, मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। मैंने तीन किताबें लिखी हैं, एक नाट्य नाटक का निर्देशन किया है और तीन वृत्तचित्र बनाए हैं, जिनमें श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि देने वाली 90 मिनट की एक फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा, मैंने दो और उपन्यास पूरे कर लिए हैं (एक का संभावित शीर्षक "द इम्परफेक्ट प्रिंस" है और दूसरा बॉलीवुड में अपने होने पर एक संस्मरण है)। मैं कभी-कभार पेंटिंग भी करता हूँ। मेरे लिए यह काम काफी है।



Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Mon, Sep 08 , 2025, 03:46 PM