
Childhood Obesity: आरव के माता-पिता हमेशा सोचते थे कि उनका चार साल का बेटा दूसरे बच्चों से बस थोड़ा बड़ा है। लेकिन जब बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट परिसर में कुछ मिनट खेलने के बाद उसकी साँस फूलने लगी, तो वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। जब उसका वज़न मापा गया, तो तराजू पर 28 किलो निकला, जो उसकी उम्र और कद के हिसाब से आदर्श वज़न से लगभग 12 किलो ज़्यादा था। डॉक्टर ने बढ़ा हुआ उपवास इंसुलिन और मेटाबॉलिक तनाव के शुरुआती लक्षण भी पाए। आईटी में काम करने वाले उसके पिता रोहन मेनन कहते हैं, "हमें लगता था कि वह बस एक स्वस्थ आहार खाता होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मोटापा एक चिकित्सा आपातकाल बन सकता है।"
आरव की कहानी भले ही असामान्य लगे, लेकिन यह भारतीय घरों में फैल रही एक शांत महामारी को दर्शाती है। लंबे समय से कुपोषण से जूझ रहे देश में, इसके विपरीत, अतिपोषण, आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा है। चूँकि बच्चे बड़े होने के साथ-साथ कद और वज़न दोनों बढ़ाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है विकास का क्रम—और कद में उसी अनुपात में वृद्धि के बिना वज़न में अचानक उछाल एक शुरुआती ख़तरे का संकेत हो सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास मानकों के अनुसार, पाँच साल से कम उम्र के बच्चे को तब अधिक वजन वाला माना जाता है जब उसकी ऊँचाई/लंबाई के अनुपात में उसका वज़न उसके आयु वर्ग और लिंग के लिए स्वस्थ औसत से दो कदम (+2 मानक विचलन, या एसडी) से ज़्यादा हो, और जब यह तीन कदम (+3 एसडी) ज़्यादा हो तो उसे मोटा माना जाता है। इसीलिए किसी बाल रोग विशेषज्ञ से बच्चे के विकास पर नज़र रखना, उसके रूप-रंग या पारिवारिक धारणा के आधार पर आकलन करने से ज़्यादा विश्वसनीय होता है।
हाल के आँकड़े बताते हैं कि शुरुआती सतर्कता क्यों ज़रूरी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) पर आधारित 2024 के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के एक अध्ययन में पाया गया कि कई राज्यों में पाँच साल से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों का अनुपात दोगुना हो गया है—पहले के दौर के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 4 प्रतिशत हो गया है। यूनिसेफ-डब्ल्यूएचओ-विश्व बैंक संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान (2025) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 3.5 प्रतिशत है, जो दो दशक पहले 1.5 प्रतिशत था।
उम्र और संपन्नता के साथ यह जोखिम बढ़ता जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 2024 में प्रकाशित एक समीक्षा में, 2007 से 2022 के बीच किए गए 21 अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 5-18 वर्ष की आयु के लगभग 71,500 स्कूली बच्चे शामिल थे। इस समीक्षा में पाया गया कि निजी स्कूलों में अधिक वजन और मोटापे की संयुक्त दर 14 प्रतिशत से अधिक है—जो सरकारी स्कूलों में दर्ज 7.2 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है। कभी पश्चिमी बीमारी समझे जाने वाला बचपन का मोटापा अब भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ते स्वास्थ्य खतरों में से एक है।
मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, साकेत में बाल चिकित्सा एंडोक्रिनोलॉजी के निदेशक डॉ. गणेश जेवालिकर इस प्रवृत्ति को "बेहद चिंताजनक" बताते हैं। क्योंकि, 'एडिपोसिटी रिबाउंड'—वह बिंदु जहाँ शरीर में वसा फिर से बढ़ने लगती है—पहले छह या सात साल की उम्र के आसपास होता था। डॉ. जेवालिकर कहते हैं, "अब यह नीचे की ओर बढ़ रहा है।" "कम उम्र में मोटापा वयस्कता में मोटापे और मेटाबोलिक सिंड्रोम के उच्च जोखिम से जुड़ा है। गैर-संचारी रोगों की घटनाओं में वृद्धि और कम उम्र में उनका होना भी बचपन के मोटापे का प्रत्यक्ष परिणाम है।"
यह सब कहाँ से शुरू होता है?
एक ऐसे देश में जहाँ कभी बच्चों के स्वास्थ्य को प्राप्त कैलोरी से मापा जाता था, अब स्थिति उलट गई है: कैलोरी पर अब नियंत्रण की आवश्यकता है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक स्पष्ट महामारी विज्ञान परिवर्तन के रूप में वर्णित करते हैं, जहाँ कुपोषण और मोटापा अब एक साथ मौजूद हैं—कभी-कभी एक ही परिवार में।
तो, इस मौन उछाल का कारण क्या है? इसकी जड़ें अक्सर बच्चे के पहला कदम—या यहाँ तक कि उसकी पहली साँस लेने से बहुत पहले ही बन जाती हैं। जिन माताओं का गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक वजन बढ़ जाता है या जिन्हें गर्भकालीन मधुमेह हो जाता है, वे भ्रूण को बढ़े हुए ग्लूकोज और इंसुलिन के स्तर के संपर्क में लाती हैं, जिससे जीवन भर के लिए चयापचय संबंधी सेट-पॉइंट बदल जाते हैं।
दिल्ली स्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनीता गुप्ता कहती हैं, "परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, मीठे पेय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरपूर मातृ आहार का संबंध शिशुओं के जन्म के समय ज़्यादा वज़न और ज़्यादा वसा (शरीर में वसा) से है।" "ऐसे शिशुओं का वज़न कम उम्र में तेज़ी से बढ़ता है, जो जन्म से पहले ही पोषण संबंधी प्रभाव का संकेत देता है।" और भारत में यह बढ़ती आवृत्ति के साथ देखा जा रहा है, वह बताती हैं।
जन्म के बाद, भोजन की आदतें इन छापों को और गहरा कर देती हैं। पहले दो वर्षों में तेज़ी से वज़न बढ़ना—खासकर उच्च-प्रोटीन फ़ॉर्मूला और ज़्यादा दूध पीने वाले शिशुओं में—बाद में मोटापे का ख़तरा बढ़ा देता है। डॉ. गुप्ता कहती हैं, "शिशु अवस्था में ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिलाना आम बात है। कई माताएँ लंबे समय तक स्तनपान कराती हैं, जबकि हर बार 20 मिनट पर्याप्त होता है। लंबे समय तक या लगातार दूध पिलाने से उल्टी, नींद में खलल और ज़्यादा कैलोरी का सेवन हो सकता है।" इसलिए, शिशुओं को खुद खाना खाने और आंतरिक भूख, या तृप्ति नियंत्रण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वह आगे कहती हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा वज़न की संस्कृति
बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रवृत्तियाँ अक्सर सांस्कृतिक मानदंडों और माता-पिता की चिंता से उपजती हैं। मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में मधुमेह और बेरिएट्रिक सर्जन डॉ. रमन गोयल कहते हैं, "दशकों से, भारत में विज्ञापन और शिशु आहार विपणन ने एक गोल-मटोल, गोल-मटोल शिशु की छवि को स्वास्थ्य की आदर्श छवि के रूप में प्रस्तुत किया है।"
"यह छवि सांस्कृतिक स्मृति में बसी हुई है। फिर भी, शैशवावस्था में अतिरिक्त वज़न स्वास्थ्य का संकेत नहीं, बल्कि चयापचय संबंधी तनाव का प्रारंभिक संकेतक है।" केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में बच्चे 2025' रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 5-9 वर्ष की आयु के एक तिहाई से ज़्यादा बच्चों में ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है—हृदय रोग के शुरुआती लक्षण—जो अतिरिक्त वज़न से जुड़े हैं।
आधुनिक जीवनशैली इन जोखिमों को और बढ़ा देती है। देर रात का खाना, मीठे नाश्ते और स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना शारीरिक गतिविधियों को दबाता है और नींद के चक्र को बिगाड़ता है—ये दोनों ही चयापचय के एक महत्वपूर्ण नियामक हैं। दिल्ली स्थित मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस, बैरिएट्रिक, जीआई एंड रोबोटिक सर्जरी के अध्यक्ष डॉ. संदीप अग्रवाल कहते हैं, "मोटापे से जुड़ी ज़्यादातर बातचीत में नींद एक अहम पहलू है। जिन शिशुओं को पर्याप्त या अच्छी नींद नहीं मिलती, उनमें भूख बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर ज़्यादा होता है और उनका वज़न ज़्यादा बढ़ता है। दुर्भाग्य से, अनियमित नींद और देर से सोना अब छोटे बच्चों में भी आम बात हो गई है।"
दो छोटे बच्चे इस समस्या को दर्शाते हैं। पुणे में, अनाया सिंह—जिनका वज़न 4.2 किलो था—को मीठा अनाज खिलाया जाता था और जब उसके माता-पिता घर से काम करते थे, तो वह घंटों कार्टून देखती थी। तीन साल की उम्र तक, उसका वज़न 18 किलो हो गया और उसमें फैटी लिवर में शुरुआती बदलाव दिखाई दिए। नोएडा में, ढाई साल के तरन, जिसे दादा-दादी मोटा बच्चा कहकर प्यार करते थे, को हर दो घंटे में दूध की बोतलें और दिन भर क्रीम बिस्कुट दिए जाते थे। उसका स्क्रीन टाइम उसके खेलने के समय से कहीं ज़्यादा था। जब उसके प्रीस्कूल के शिक्षकों ने लगातार प्यास और कम ध्यान देने की आदत देखी, तो रक्त परीक्षण में लिवर एंजाइम्स में वृद्धि का पता चला।
दिनचर्या में बदलाव
डॉ. गोयल के अनुसार, ज़्यादातर माता-पिता यह सोचते ही नहीं कि शिशु का वज़न ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण वे कम रिपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं, "शिशुओं को उनके खाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हर कैलोरी उन्हें खिलाने वाले वयस्कों से आती है। वयस्कों में, हम इच्छाशक्ति या जीवनशैली की बात कर सकते हैं, लेकिन शिशुओं में, मोटापा घर की आदतों को दर्शाता है।"
बड़े बच्चों के लिए GLP-1 एगोनिस्ट जैसी नई मोटापा-रोधी दवाओं का दुनिया भर में परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज उनके परिवेश और दिनचर्या के ज़रिए ही सबसे अच्छा होता है (देखें ट्रिगर और समाधान)। डॉ. अग्रवाल कहते हैं, "ज़्यादातर छोटे बच्चों में मोटापे का कोई निश्चित इलाज नहीं है।" "अत्यंत गंभीर मामलों में, सर्जरी एक दयालु, जीवन रक्षक उपाय बन जाती है, लेकिन ये असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं। जो कारगर होता है वह है निरंतर व्यवहारिक हस्तक्षेप—सुगठित दिनचर्या, ध्यानपूर्वक भोजन, पर्याप्त नींद और शारीरिक खेल। पारिवारिक स्तर पर आदतों को बदलना किसी भी चिकित्सा से कहीं ज़्यादा प्रभावी है।"
प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं। चिकित्सा पत्रिका क्यूरियस में भारतीय रोकथाम रणनीतियों की 2024 की समीक्षा में पाया गया कि पोषण परामर्श, सक्रिय खेल और स्क्रीन-टाइम में कमी को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण पूर्वस्कूली सेटिंग्स में व्यवहार्य और प्रभावी था। नीति जंक फूड के विपणन पर अंकुश लगाकर, खेल के स्थानों में सुधार करके और माता-पिता को शिक्षित करके मदद कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव घर पर ही होना चाहिए।
उत्साहजनक तथ्य यह है कि छोटे बच्चे जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। उनका जीव विज्ञान अनुकूलनशील होता है, उनकी आदतें अभी भी लचीली होती हैं। शुरुआती हस्तक्षेप—खासकर स्कूल के वर्षों से पहले—स्थायी परिणाम दे सकते हैं। अंततः, सफलता केवल तराजू पर ही नहीं दिखाई देगी। यह बच्चे की ऊर्जा, आत्मविश्वास और गति में आनंद में दिखाई देगी—एक ऐसे बचपन के चिह्न जो अति से नहीं, बल्कि संतुलन से परिभाषित होता है।

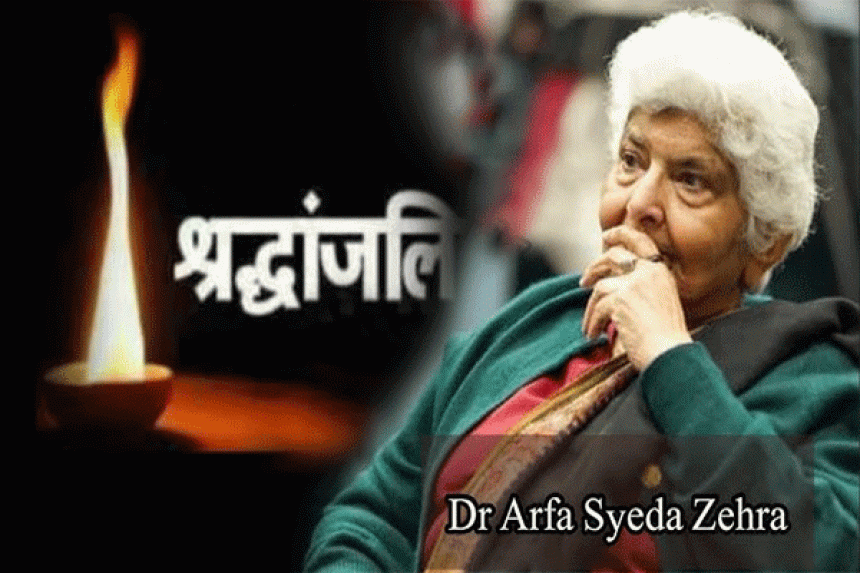

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Wed, Nov 12 , 2025, 09:49 AM